कविता प्रकृति से ही केन्द्राभिसारी (centrifugal) होती है। इस युग में भी, जब 'सन्तन' को 'सीकरी' से काम पड़ जाता है कभी-कभी, और 'फकीर' बने रहने का आत्मबल नहीं जुटा पाते साहित्यकार-व्यवस्था-विरोध का तेज उनमें होता है। ऐसे में 'व्यवस्था', 'प्रबन्धन' या 'सत्ता' से जुड़े लोग जब कविता लिखते हैं- उन्हें आत्मालोचन, संशयात्मक विश्लेषण के वे ही आघात झेलने होते हैं जो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'गोरा' ने झेले थे!
कविता एक सार्वजनिक आँगन है-'चौराहा' और 'देहली' के बीच की जगह! चूँकि वह सबका 'स्पेस' है-'घुसपैठिया' वहाँ कोई होता नहीं ! जैसे कोई 'गा' सकता है, कोई 'लिख' भी सकता है! एक हाइड-पार्क है कविता! खिड़की खोलने का मूलाधिकार आप किसी से भी कैसे छीन सकते हैं ? वैकल्पिक विश्व की एक 'तड़प' तो सबके भीतर होती है- 'संज्ञा' की विडम्बनाएँ करीब से देखने वालों के भीतर क्यों नहीं हों भला ?
बड़े शहरों के 'गरीब' और कस्बों के निम्न मध्यवर्गीय 'मुहल्लों' में एक दृश्य आम होता है! फुटपाथ पर ही 'खाट' या 'मचिया' बिछी है-हुक्का सजा है, धूप में सब्जियाँ कतरी जा रही हैं, हो रहा है-विचार-विनिमय, बच्चे 'डेंगा-पानी' खेल रहे हैं! फुटपाथ पर बँधी गायें भी रँभा रही हैं.... चल रहा है जीवन-चक्र और जीवन का गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला भी !
जीवन के गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला ही है कविता- यहीं से विकासजी की कविताओं के सूत्र भी पकड़े जा सकते हैं। सार्वजनिक खाट की तरह ही उन्होंने 'कुर्सी' फुटपाथ पर उतारी है। राजनीतिक प्रभुता की एक सत्ता होती होगी, पर उसके समानांतर सांस्कृतिक जीवन की सत्ता कम महत्त्वपूर्ण नहीं। सुनहरे पाए वाली एक सुनहरी कुर्सी के बरक्स सुतली और मूँज की तिपाइयाँ कम बड़ा 'आसन' नहीं। सच्चे सिंहासन तो मूँज की तिपाइयाँ हैं-विकासजी की कविता ये ही समझने की ताकत पैदा करती हैं! सहज बातचीत की लय में बढ़ने वाली ये छोटी-बड़ी कविताएँ हैं तो विमर्श प्रधान किन्तु बोझिल नहीं ! आत्ममंथन से अधिक ये 'पर्यवेक्षण' की कविताएं हैं! विज्ञान के विद्यार्थी जैसी तटस्थता से वे अपनी प्रैक्टिकल फाइल के तीन कॉलम बनाते हैं—प्रयोग-निरीक्षण और निष्कर्ष - उनकी कविता जीवन को तर्क निकष पर कसती है ! अलग-अलग जीवन-सन्दर्भ कविता में नए ढंग से अनुस्यूत कैसे हो सकते हैं- इसके दो खूबसूरत उदाहरण 'शंघाई' और 'यूटोपिया' हैं।
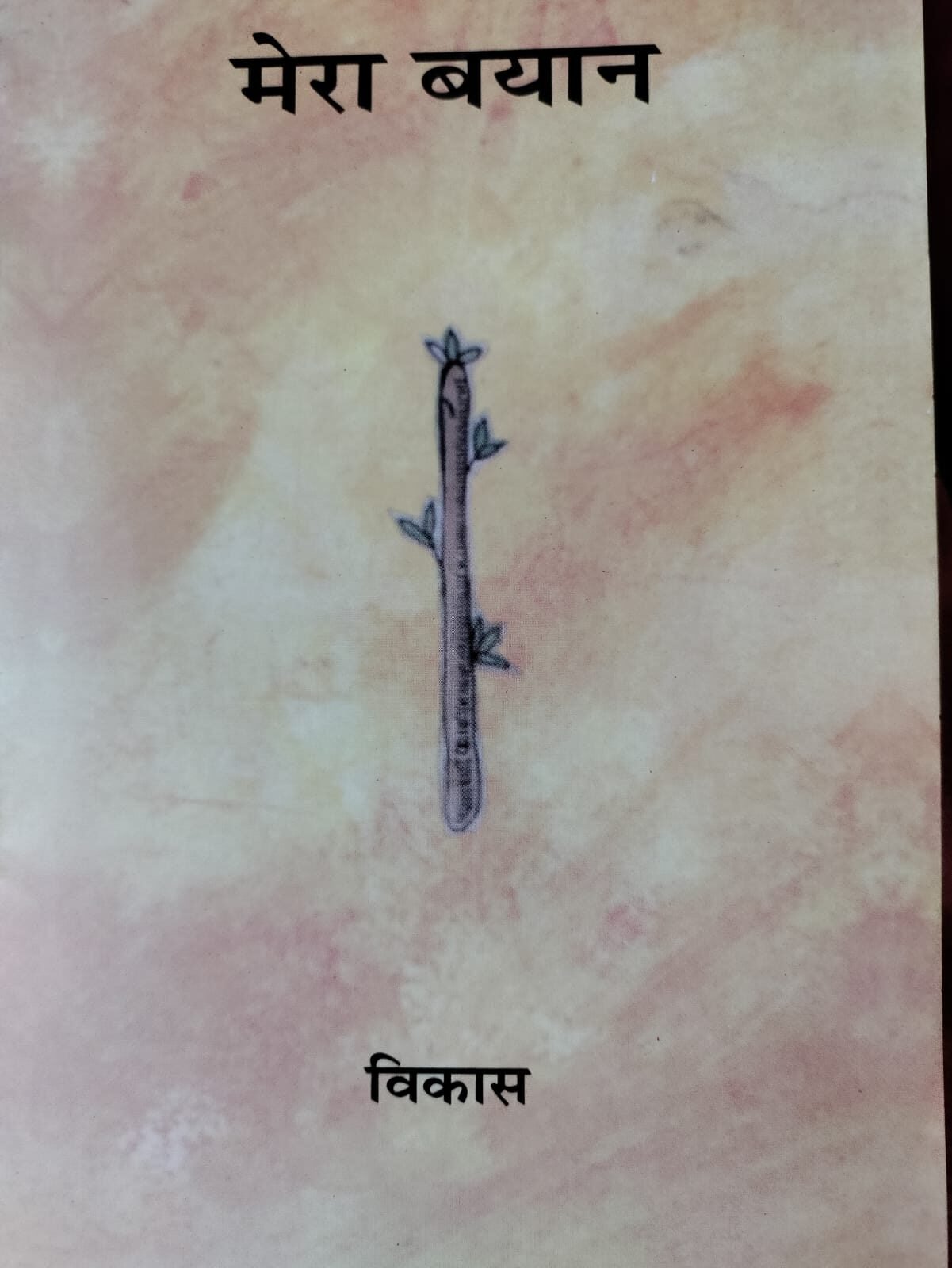 कविता प्रकृति से ही केन्द्राभिसारी (centrifugal) होती है। इस युग में भी, जब 'सन्तन' को 'सीकरी' से काम पड़ जाता है कभी-कभी, और 'फकीर' बने रहने का आत्मबल नहीं जुटा पाते साहित्यकार-व्यवस्था-विरोध का तेज उनमें होता है। ऐसे में 'व्यवस्था', 'प्रबन्धन' या 'सत्ता' से जुड़े लोग जब कविता लिखते हैं- उन्हें आत्मालोचन, संशयात्मक विश्लेषण के वे ही आघात झेलने होते हैं जो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'गोरा' ने झेले थे! कविता एक सार्वजनिक आँगन है-'चौराहा' और 'देहली' के बीच की जगह! चूँकि वह सबका 'स्पेस' है-'घुसपैठिया' वहाँ कोई होता नहीं ! जैसे कोई 'गा' सकता है, कोई 'लिख' भी सकता है! एक हाइड-पार्क है कविता! खिड़की खोलने का मूलाधिकार आप किसी से भी कैसे छीन सकते हैं ? वैकल्पिक विश्व की एक 'तड़प' तो सबके भीतर होती है- 'संज्ञा' की विडम्बनाएँ करीब से देखने वालों के भीतर क्यों नहीं हों भला ? बड़े शहरों के 'गरीब' और कस्बों के निम्न मध्यवर्गीय 'मुहल्लों' में एक दृश्य आम होता है! फुटपाथ पर ही 'खाट' या 'मचिया' बिछी है-हुक्का सजा है, धूप में सब्जियाँ कतरी जा रही हैं, हो रहा है-विचार-विनिमय, बच्चे 'डेंगा-पानी' खेल रहे हैं! फुटपाथ पर बँधी गायें भी रँभा रही हैं.... चल रहा है जीवन-चक्र और जीवन का गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला भी ! जीवन के गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला ही है कविता- यहीं से विकासजी की कविताओं के सूत्र भी पकड़े जा सकते हैं। सार्वजनिक खाट की तरह ही उन्होंने 'कुर्सी' फुटपाथ पर उतारी है। राजनीतिक प्रभुता की एक सत्ता होती होगी, पर उसके समानांतर सांस्कृतिक जीवन की सत्ता कम महत्त्वपूर्ण नहीं। सुनहरे पाए वाली एक सुनहरी कुर्सी के बरक्स सुतली और मूँज की तिपाइयाँ कम बड़ा 'आसन' नहीं। सच्चे सिंहासन तो मूँज की तिपाइयाँ हैं-विकासजी की कविता ये ही समझने की ताकत पैदा करती हैं! सहज बातचीत की लय में बढ़ने वाली ये छोटी-बड़ी कविताएँ हैं तो विमर्श प्रधान किन्तु बोझिल नहीं ! आत्ममंथन से अधिक ये 'पर्यवेक्षण' की कविताएं हैं! विज्ञान के विद्यार्थी जैसी तटस्थता से वे अपनी प्रैक्टिकल फाइल के तीन कॉलम बनाते हैं—प्रयोग-निरीक्षण और निष्कर्ष - उनकी कविता जीवन को तर्क निकष पर कसती है ! अलग-अलग जीवन-सन्दर्भ कविता में नए ढंग से अनुस्यूत कैसे हो सकते हैं- इसके दो खूबसूरत उदाहरण 'शंघाई' और 'यूटोपिया' हैं।
कविता प्रकृति से ही केन्द्राभिसारी (centrifugal) होती है। इस युग में भी, जब 'सन्तन' को 'सीकरी' से काम पड़ जाता है कभी-कभी, और 'फकीर' बने रहने का आत्मबल नहीं जुटा पाते साहित्यकार-व्यवस्था-विरोध का तेज उनमें होता है। ऐसे में 'व्यवस्था', 'प्रबन्धन' या 'सत्ता' से जुड़े लोग जब कविता लिखते हैं- उन्हें आत्मालोचन, संशयात्मक विश्लेषण के वे ही आघात झेलने होते हैं जो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'गोरा' ने झेले थे! कविता एक सार्वजनिक आँगन है-'चौराहा' और 'देहली' के बीच की जगह! चूँकि वह सबका 'स्पेस' है-'घुसपैठिया' वहाँ कोई होता नहीं ! जैसे कोई 'गा' सकता है, कोई 'लिख' भी सकता है! एक हाइड-पार्क है कविता! खिड़की खोलने का मूलाधिकार आप किसी से भी कैसे छीन सकते हैं ? वैकल्पिक विश्व की एक 'तड़प' तो सबके भीतर होती है- 'संज्ञा' की विडम्बनाएँ करीब से देखने वालों के भीतर क्यों नहीं हों भला ? बड़े शहरों के 'गरीब' और कस्बों के निम्न मध्यवर्गीय 'मुहल्लों' में एक दृश्य आम होता है! फुटपाथ पर ही 'खाट' या 'मचिया' बिछी है-हुक्का सजा है, धूप में सब्जियाँ कतरी जा रही हैं, हो रहा है-विचार-विनिमय, बच्चे 'डेंगा-पानी' खेल रहे हैं! फुटपाथ पर बँधी गायें भी रँभा रही हैं.... चल रहा है जीवन-चक्र और जीवन का गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला भी ! जीवन के गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला ही है कविता- यहीं से विकासजी की कविताओं के सूत्र भी पकड़े जा सकते हैं। सार्वजनिक खाट की तरह ही उन्होंने 'कुर्सी' फुटपाथ पर उतारी है। राजनीतिक प्रभुता की एक सत्ता होती होगी, पर उसके समानांतर सांस्कृतिक जीवन की सत्ता कम महत्त्वपूर्ण नहीं। सुनहरे पाए वाली एक सुनहरी कुर्सी के बरक्स सुतली और मूँज की तिपाइयाँ कम बड़ा 'आसन' नहीं। सच्चे सिंहासन तो मूँज की तिपाइयाँ हैं-विकासजी की कविता ये ही समझने की ताकत पैदा करती हैं! सहज बातचीत की लय में बढ़ने वाली ये छोटी-बड़ी कविताएँ हैं तो विमर्श प्रधान किन्तु बोझिल नहीं ! आत्ममंथन से अधिक ये 'पर्यवेक्षण' की कविताएं हैं! विज्ञान के विद्यार्थी जैसी तटस्थता से वे अपनी प्रैक्टिकल फाइल के तीन कॉलम बनाते हैं—प्रयोग-निरीक्षण और निष्कर्ष - उनकी कविता जीवन को तर्क निकष पर कसती है ! अलग-अलग जीवन-सन्दर्भ कविता में नए ढंग से अनुस्यूत कैसे हो सकते हैं- इसके दो खूबसूरत उदाहरण 'शंघाई' और 'यूटोपिया' हैं।