मुझे यह कहना ही चाहिये कि यह एक जरूरी विषय को केन्द्र में रख कर लिखी गयी, एक जरूरी किताब है। मुझे इस बात की खास खुशी हुई कि दीपचन्द्र निर्मोही जी इतने निर्मोही नहीं निकले कि इस जरूरी काम से मुँह मोड़ लें। मैं मानता हूँ कि सभी गाँधीजनों का यह धर्म है कि वे गाँधी को ज्यादा-से-ज्यादा पढ़ें, समझें और समाज तक पहुँचाएँ। उस बेचारे गाँधी को हमने गोली ही नहीं मारी, दूसरी कई तरहों से भी उन्हें मारा है जिसमें उन्हें ठीक तरह से न समझना भी शामिल है। इसलिए भी यह किताब गाँधी के नमक का कर्ज अदा करने जैसी है।
गाँधी की हत्या अब इतिहास में दफन हो चुकी सच्चाई है। हमने उस कोई 80 साल के बूढ़े आदमी को तीन गोलियों से बींध दिया था। गाँधी मार डाले गये और उनका अन्तिम संस्कार भी हमने कर दिया। लेकिन गाँधी उन तीन गोलियों से मरे नहीं, यह बात हम भी जानते हैं जो गाँधी को मानते हैं; वे भी जानते हैं जो गाँधी को मारते हैं। जो गाँधी को मानते हैं वे अपने भरसक उनके मूल्यों को जिन्दा रखने में लगे हैं; जो गाँधी के विफल हत्यारे हैं वे कभी उनकी मूर्ति को तो कभी उनके फोटो आदि को मार कर देखते रहते हैं कि इससे यह आदमी मरता है या नहीं। तो जिन्दगी और मौत की ताकतों के बीच एक रस्साकशी-सी चल रही है। दीपचन्द्र निर्मोही जी जैसे लोग उन्हें मरने देने को तैयार नहीं हैं; सावरकर वाले उन्हें जीने की इजाजत देने को तैयार नहीं हैं। यह किताब इसी रस्साकशी का परिणाम है।
दीपचन्द्र जी को इस बात का पूरा श्रेय है कि वे गाँधी से अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कोई संशय रहने नहीं देते हैं फिर भी हत्यारे पक्ष के प्रति पूरी उदारता व सदाशयता बरत पाते हैं। उन्होंने बहुत स्रोतों से, बहुत सारे तथ्य जुटा कर हमारे सामने रख दिये हैं और किताब हमें सौंप कर, यह कहते हुए पीछे हट गये हैं कि अब निष्कर्ष आपका ! यह कठिन कसरत बन जाती है क्योंकि हम पाते हैं कि इतिहास की किताबें खोल कर भी लोग न इतिहास जान पाते हैं, न समझ पाते हैं। इसलिये भी इस किताब को पढ़ना एक चुनौती बन जाती है कि इससे आप खुद को जाँच सकते हैं कि दीपचन्द्रजी की किताब पढ़ कर आप सत्य तक पहुँच पाते हैं या नहीं। सच के बारे में हमारे एक शायर ने बड़े पते की एक बात लिखी
है- “सच घटे या बढे तो सच न रहे/झठ की कोई इंतहा ही नहीं।” कमोवेश ऐसा ही इतिहास के बारे में भी है। जो लिखा गया इतिहास है, वह आधा ही बताता है। बाकी परी तस्वीर बगैर कुछ जोड़े या छोड़े, आपको खुद ही समझनी व आंकनी पड़ती है।
फासिज्म का चरित्र भी कुछ ऐसा ही है। उसका एक लक्षण यह है कि वह पूरी तरह सामने आता नहीं है। सावरकर को और हिन्दुत्व के सारे पैरोकारों को समझने में इतिहास के सामान्य पाठकों को यही दिक्कत आती है। वे कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पाप-पुण्य के नाम पर, कभी संस्कृति और राष्ट्र के नाम पर आवाज लगाते हैं लेकिन अपना असली मकसद छिपा कर रखते हैं। यह किताब उस असली मकसद को समझने में हमारी मदद करती है।
गाँधी का सन्दर्भ लेते हुए कई लोगों और कई प्रसंगों को स्वाभाविक विस्तार से लेखक ने लिखा है जिससे यह किताब गाँधी तक सीमित नहीं रह जाती है बल्कि कई स्थितियों को, कई गाँठों को समझने में हमारी मदद करती है। वन्दे मातरम् गान का पूरा सन्दर्भ देते हुए दीपचन्द्रजी जिस तरह बंकिम बाबू और उनके उपन्यास ‘आनन्दमठ’ को समझते व समझाते हैं, वह सब जानना बहुत जरूरी है। इससे यह समझना भी आसान हो जाता है कि गाँधीजी ने कैसी विकट चुनौतियों के बीच से भारतीय समाज की एकता को संभाल कर आजादी तक पहुँचाया था अन्यथा गृहयुद्ध की आग में जल कर गुलामी की हमारी बेड़ियाँ और भी मजबूत हो जातीं। अँग्रेजी राज को अपना अहोभाग्य समझने वालों में बंकिम बाबू अकेले नहीं थे बल्कि एक पूरा दर्शन ही उनके समर्थन में खड़ा हुआ था जिसे गाँधी को साथ भी लेना था और उसके विषदत भी तोड़ने थे।
मनुस्मृति के सन्दर्भ में लेखक हमें भारतीय जाति-व्यवस्था के भीतर ले जाता है। यह पुस्तक का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। साम्प्रदायिक दुराव व जाति-प्रथा, ये दो ताकतें थीं जिनसे गाँधी ताउम्र जूझते रहे और हम कह सकते हैं कि इन दोनों ताकतों ने ही उनको लील भी लिया। भगवान बुद्ध के बाद जाति-व्यवस्था के खिलाफ जैसा विकट अभियान गाँधीजी ने छेड़ा, उसका सानी दूसरा कहीं मिलता नहीं है। भारतीय समाज का विघटन बचाते हुए वे इस अभियान को जितनी दूर तक और जितनी ऊँचाई तक ले जा सके, वह चमत्कार सरीखा लगता है। यह रचनात्मक विरोध गाँधीजी की अहिंसक कला के कारण ही सम्भव हुआ था।
शिवाजी के कालखंड की, हिन्दी भाषा के जन्म व विकास की कहानी भी अत्यन्त सारगर्भित है। सावरकर और हिन्दुत्व के पूरे प्रसंग को भी लेखक ने
प्रमाणों के साथ बड़ी बेबाकी से दर्ज किया है। जब आप किताब पूरी करते हैं तब आपको एक ज्ञान-यज्ञ से गुजरने का अहसास होता है। इसके पाठकों व चाहकों की संख्या बढ़े और वे वर्तमान भारत की चुनौतियों व खतरों को समझ भी सकें और उनका सामना भी कर सकें, इस कामना के साथ मैं यह किताब आपके हाथों में सौंपता हूँ।
कुमार प्रशान्त
15 अगस्त, 2021
गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान,

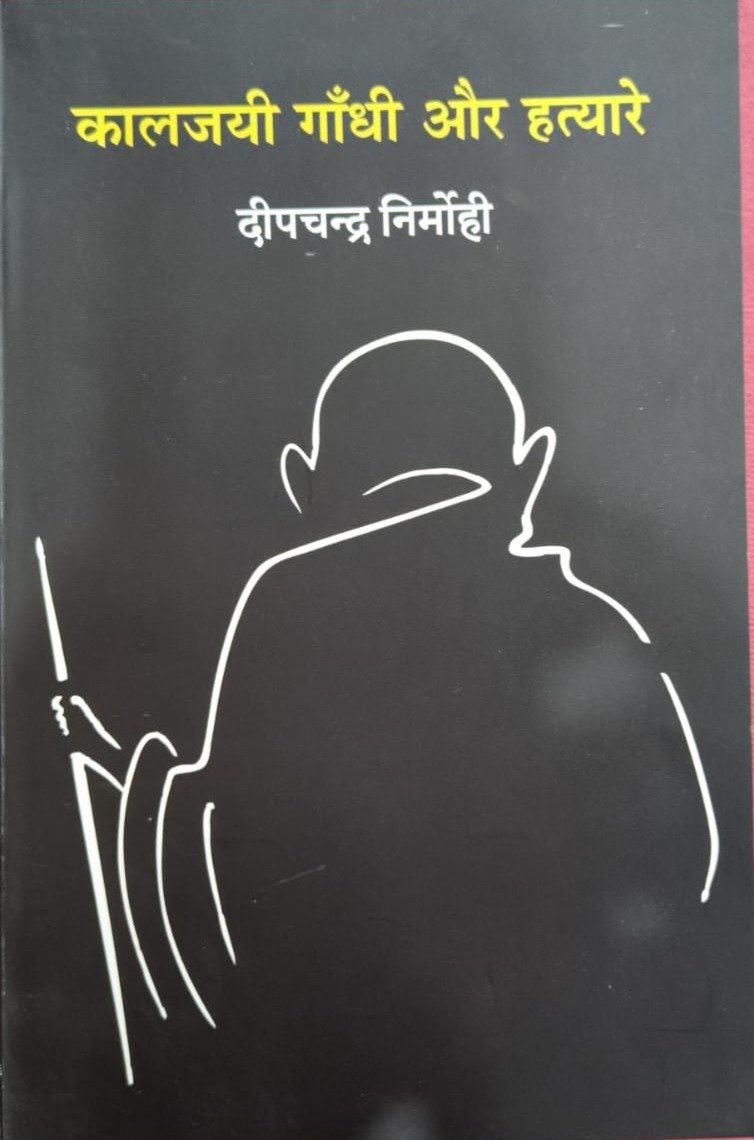

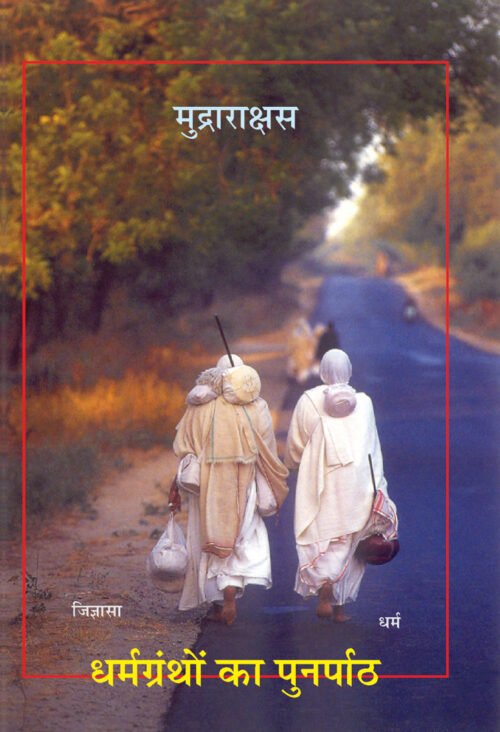


Reviews
There are no reviews yet.